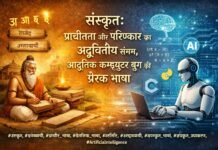देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मन की बात’ कभी रेडियो का सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम हुआ करती थी। महीने का आख़िरी रविवार आता नहीं था कि समर्थक ट्रांजिस्टर लेकर तैयार और आईटी सेल ट्वीट लेकर तत्पर। लेकिन अब लगता है कि “मन” तो है, पर “बात” कहीं खो गई है।
भाषणों में बड़े-बड़े विज़न, विश्वगुरु का सपना, अमृतकाल का उद्घोष—सब कुछ है। पर जब सवाल ज़मीन से उठते हैं—महंगाई की मार, बेरोज़गारी की कतार, किसान की पुकार—तो रेडियो की तरंगें अचानक धीमी पड़ जाती हैं। लगता है जैसे “मन की बात” अब “मन की राहत” बन गई हो—ऐसी बातें जो सुनने में सुकून दें, पर जवाबदेही से दूरी बनाए रखें। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में उबाल है। विश्वविद्यालयों में बहस है, सोशल मीडिया पर बवाल है, सड़कों पर सवाल है। भाजपा का परंपरागत सवर्ण वोटर, जो कभी “सबका साथ” के नारे में खुद को अग्रिम पंक्ति में देखता था, आज बेचैन दिखाई देता है। नाराज़गी के स्वर दबे नहीं हैं—बस मंच की तलाश में हैं।
लेकिन “मन की बात” में इन सवालों की एंट्री नहीं होती। वहां प्रेरक कहानियाँ हैं, स्टार्टअप के किस्से हैं, विदेशी मंचों की तालियाँ हैं। मगर जब कोर वोटर ही आक्रोश में हो, तब संवाद का साहस कहाँ है?
विडंबना देखिए—जिस कार्यक्रम को सीधा संवाद कहा गया, वह दरअसल एकतरफा प्रसारण निकला। जनता सुनती है, प्रधानमंत्री बोलते हैं। लेकिन जनता पूछ नहीं सकती। और जब पूछने का माहौल बनता है, तब कार्यक्रम की आवृत्ति ही कम हो जाती है। आज हालात ऐसे हैं कि लोग पूछ रहे हैं—क्या “मन की बात” अब केवल तब होगी जब मन प्रसन्न हो? क्या कठिन प्रश्नों का सामना करना नेतृत्व की परिभाषा में शामिल नहीं?
राजनीति में भाषण देना आसान है, लेकिन असंतोष का सामना करना कठिन। आक्रोशित समर्थकों को समझाना उससे भी कठिन। और शायद यही वजह है कि इन दिनों “मन की बात” की आवाज़ कुछ धीमी-सी लगती है।
देश को प्रेरणा की कहानियाँ जरूर चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे भरोसे की ज़रूरत है। अगर “मन की बात” सच में मन से होती, तो शायद आज सड़कों पर सवाल कम और संवाद अधिक दिखता।
क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तालियाँ नहीं, बल्कि सवाल होते हैं। और जब सवाल बढ़ते हैं, तो खामोशी सबसे बड़ा बयान बन जाती है।
यूजीसी नियम पर उठे सवाल: क्या भाजपा अपनी ही विचारधारा से भटक रही है?